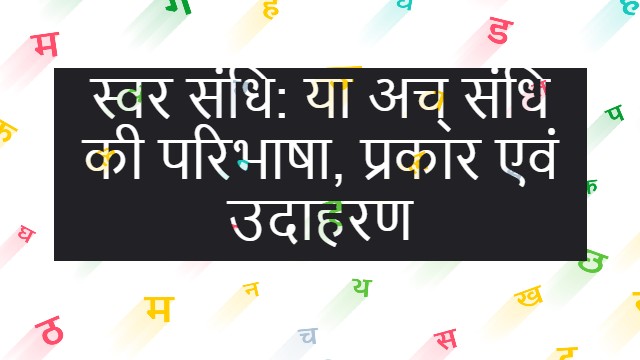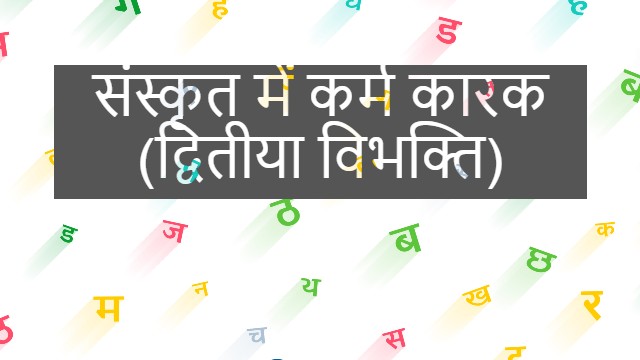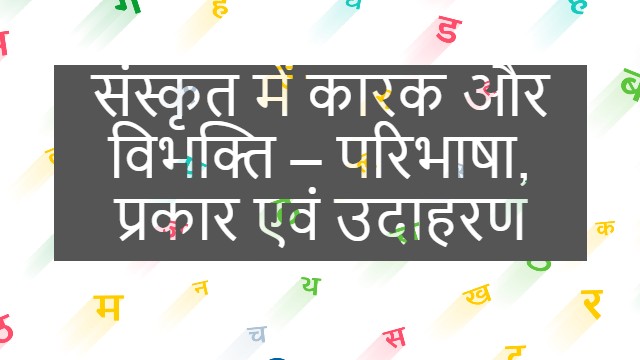सन्धि
शब्दों के उच्चारण में जिह्वा एक शब्द के उच्चारण के पश्चात् दूसरे शब्द का उच्चारण करती है अतः प्रथम शब्द का अन्तिम स्वर व्यंजन अथवा विसर्ग द्वितीय शब्द के प्रारम्भिक स्वर अथवा व्यंजन से प्रभावित होते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन व्याकरण में सन्धि का रूप ग्रहण करता है।
सन्धि तीन प्रकार की होती है-
१. स्वर सन्धि या अच् सन्धि ।
२. व्यंजन सन्धि या हल् सन्धि ।
स्वर अथवा अच् सन्धि (संस्कृत में)
प्रथम शब्द के अन्तिम स्वर के साथ दूसरे शब्द के आदि स्वर के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर सन्धि कहते हैं। जैसे- विद्या अर्थी = विद्यार्थी। यहाँ ‘द्या’ के अन्त में आने वाला ‘आ’ और ‘अर्थी’ के आदि में आने वाले ‘अ’ को मिलाकर ‘आ’ हो गया है।
‘आ’ तथा ‘अ’ दोनों ही स्वर हैं, अतः विद्यार्थी’ में स्वर सन्धि है।
विशेष-स्वर सन्धि करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यंजन आधे लिखे हुए नहीं होते और उनके अन्त में ( ् ) चिन्ह लगा हुआ नहीं होता अर्थात् जो ‘हलन्त’ नहीं होते, वे सभी अपने अन्त में किसी न किसी स्वर को अवश्य रखते हैं। जैसे-‘क’ में ‘अ’, कि’ में ‘इ’, ‘कु’ में ‘उ’ और ‘कृ’ में ‘ऋ’ है।
स्वर सन्धि प्रधानतः छः प्रकार की होती है-
(१) दीर्घ स्वर सन्धि
(२) गुण स्वर सन्धि
(३) वृद्धि स्वर सन्धि
(४) यण् स्वर सन्धि
(५) अयादि स्वर सन्धि
(६) पूर्व रूप स्वर सन्धि
१. दीर्घ स्वर सन्धि
सूत्र– अकः सवर्णे दीर्घः।
ऊपर लिखा जा चुका है कि ‘अ’ और ‘आ’, ‘इ’ और ‘ई’, ‘उ’ और ‘ऊ’ तथा ‘ऋ’ और ‘ऋ’ ‘लृ’ आपस में समान स्वर या सवर्ण हैं। जब यह समान या सवर्ण स्वर पास-पास आ जाते हैं, तब वे दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। नीचे के विवरण में विभिन्न नियमों द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। विद्यार्थी इन नियमों को भली भाँति समझकर याद कर लें।
नियम (क) — यदि ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘अ’ या ‘आ’ आये तो दोनों के स्थान पर ‘आ’ हो जाता है।
नोट- प्रथम शब्द का अन्तिम स्वर व्यंजनों पर मात्रा के रूप में तथा दूसरे शब्द का आदि वर्ण मूल स्वर के रूप में आता है। सन्धि होने पर मूल स्वर दीर्घ मात्रा के रूप में आ जाता है। जैसे-
अ + अ = आ, धन + अर्थी = धन् + अ + अर्थी = धनार्थी
अ + आ = आ, हिम + आलयः = हिम् + अ + आलय = हिमालयः ।
आ + अ = आ, विद्या + अर्थी = विद्य् + आ + अर्थी = विद्यार्थी ।
आ + आ = आ, विद्या+आलयः = विद्य् + आ + आलयः = विद्यालयः ।
नियम (ख) — यदि ‘इ’ या ‘ई’ के बाद ‘इ’ या ‘ई’ आये तो दोनों के स्थान पर ‘ई’ हो जाती है।
जैसे-
इ + इ = ई, गिरि + इन्द्रः = गिर् + इ + इन्द्रः = गिरीन्द्रः ।
इ + ई = ई, कपि + ईशः = कप् + इ + ईशः = कपीशः ।
ई + इ = ई, मही + इन्द्रः = मह् + ई + इन्द्रः = महीन्द्रः ।
ई + ई = ई, श्री + ईशः = श्र + ई + ईशः = श्रीशः ।
नियम (ग) — यदि ‘उ’ या ‘ऊ’ के बाद ‘उ’ या ‘ऊ’ आये तो दोनों के स्थान पर ‘ऊ’ हो जाता है।
जैसे-
उ + उ = ऊ, भानु + उदयः = भान् + उ + उदयः = भानूदयः ।
उ + ऊ = ऊ, लघु + ऊर्मिः = लघ् + उ + ऊर्मिः = लघूर्मिः ।
ऊ + उ = ऊ, वधू + उन्नतिः = वध् + ऊ + उन्नतिः = वधून्नतिः ।
ऊ + ऊ = ऊ, वधू + ऊर्मि = वध्+ ऊ + ऊर्मिः = वधूर्मिः
नियम (घ)– यदि ऋ, ऋ के बाद ऋ या ऋ आये तो ऋ हो जाता है। लृ का प्रयोग न के बराबर है। लृ का ॠ हो जाता है।
जैसे-
ऋ + ऋ = ऋ, पितृ + ऋणाम् = पित् + ऋ ऋणाम् = पितृणाम् ।
होतृ + ऋकारः = ऋ + ऋ = ऋ = होत् + ऋ + ऋकारः = होतृकारः ।
नोट-ऊपर कहे हुए चारों नियमों को एक करके नीचे लिखा हुआ एक नियम बन जाता है।
यदि हस्व या दीर्घ ‘अ, इ, उ, ऋ और लृ’ के बाद उनके सवर्ण स्वर आयें तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः ‘आ, ई, ऊ, ऋ’ हो जाते हैं।
२. गुण स्वर सन्धि
सूत्र-आद्गुणः।
नियम (क) — यदि ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘इ या ई’ आये तो दोनों के स्थान में ‘ए’ हो जाता है।
जैसे-
अ + इ = ए, सुर + इन्द्रः = सुर् + अ + इन्द्रः = सुर् + एन्द्रः = सुरेन्द्रः ।
अ + ई= ए, सुर + ईशः = सुर् + अ + ईशः = सुर् + एशः = सुरेशः ।
आ + इ = ए, महा + इन्द्रः = मह् + आ + इन्द्रः = मह् + एन्द्रः = महेन्द्रः ।
आ + ई = ए, महा + ईश्वरः = मह् + आ + ईश्वरः = मह् + एश्वरः = महेश्वरः ।
नियम (ख) — यदि ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘उ’ या ‘ऊ’ आये तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है।
जैसे-
अ +उ = ओ, सूर्य + उदयः = सूर्य + अ + उदयः = सूर्य + ओदयः = सूर्योदयः ।
अ + ऊ = ओ, तव + ऊर्मिः = तव् + अ + ऊर्मिः = तव् + ओर्मिः = तवोर्मिः ।
आ + उ = ओ, गंगा + उदकम् = गंग् + आ + उदकम् = गंग् + ओदकम् = गंगोदकम् ।
आ + ऊ = ओ, यमुना + ऊर्मयः = यमुन् + आ + ऊर्मयः = यमुन् + ओर्मयः = यमुनोर्मयः ।
नियम (ग) — यदि ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘ऋ’ आये तो दोनों के स्थान पर ‘अर्’ हो जाता है।
जैसे-
अ + ऋ = अर्, देव + ऋषिः = देव् + अ + ऋषिः = देव् + अर् + षिः = देवर्षिः
आ + ऋ = अर्, महा + ऋषिः = मह् + आ + ऋषि = मह् + अर् + षिः = महर्षिः
नियम (घ) — यदि ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘लृ’ आये तो दोनों के स्थान पर ‘अल्’ हो जाता है।
जैसे-
अ + लृ = अल्, तव + लृकारः = तव् + अ + लृकारः = तव् + अल् + कार = तवल्कारः ।
नोट- ऊपर के चारों नियमों को एकत्र करने पर नीचे लिखा हुआ एक नियम बन जाता है।
यदि अ या आ के बाद इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ या लृ आये तो उन दोनों के स्थान पर अ या आ + इ या ई = ए, अ या आ + उ या ऊ = ओ, अ या आ + ऋ या ऋ = अर् और अ या आ + लृ = अल् हो जाते हैं।
३. वृद्धि स्वर सन्धि
सूत्र- वृद्धिरेचि ।
नियम (क) — यदि ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘ए’ या ‘ऐ’ हो तो दोनों के स्थान पर ‘ऐ’ हो जाता है
जैसे-
अ + ए = ऐ, मम + एकता = मम् + अ + एकता = मम् + ऐकता = ममैकता ।
आ + ए = ऐ, सदा + एव = सद् + आ + एव = सद् + ऐव = सदैव ।
आ + ऐ = ऐ, तव + ऐश्वर्यम् = तव् + अ + ऐश्वर्यम् = तव् + ऐश्वर्यम् = तवैश्वर्यम् ।
आ + ऐ = ऐ, सदा = ऐक्यम् = सद् + आ + ऐक्यम् = सद् + ऐक्यम् = सदैक्यम् ।
नियम(ख) — यदि ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘ओ’ ‘औ’ आये तो दोनों का मिलकर ‘औ’ हो जाता है।
जैसे-
अ +ओ = औ, जल + ओघः = जल् + अ + ओघः = जल् + औघः = जलौघः ।
आ + ओ = औ, महा + ओजः = मह् + आ + ओजः = मह् + औजः = महौजः ।
अ + औ = औ, वन + औषधम् = वन् + अ + औषधम् = वन् + औषधम् = वनौषधम् ।
आ + औ = औ, महा + औषधम् = मह् + आ + औषधम् = मह् + औषधम् = महौषधम् ।
नोट-उक्त नियमों को मिलाने से नीचे लिखा नियम बनता है-
यदि ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘ए’ या ‘ऐ’ आये तो दोनों मिलकर ‘ऐ’ और ‘ओ’ या ‘औ’ आये तो दोनों मिलकर ‘औ’ हो जाते हैं।
४. यण् स्वर सन्धि
सूत्र – इकोयणचि ।
नियम (क) — यदि ‘इ’ या ‘ई’ के बाद कोई असमान स्वर आये, तो ‘इ’ या ‘ई’ का ‘य्’ हो जाता है।
जैसे-
इ + आ = य् + आ = या, इति + आदिः = इत् + इ + आदिः = इत् + य् + आदिः = इत्यादिः ।
ई + ओ = य् + ओ = यो, नदी + ओघः = नद् + ई + ओघः = नद् + य् +ओघः = नद्योघः ।
नियम (ख) — यदि ‘उ’ या ‘ऊ’ के बाद कोई असमान स्वर आये, तो ‘उ’ ‘ऊ’ का ‘व्’ हो जाता है।
जैसे-
उ + आ = व् + आ = वा, सु + आगतम् = स् + उ + आगतम् = स् + व् + आगतम् = स्वागतम् ।
ऊ + आ = व् + आ = वा, वधू + आगमनम् = वधू + ऊ + आगमनम् = वधू + व् + आगमनम् = वध्वागमनम् ।
नियम (ग) — यदि ‘ऋ’ के बाद कोई असमान स्वर आये, तो ऋ’ का ‘र्’ हो जाता है ।
जैसे-
ऋ + आ = र् + आ = रा, पितृ + आज्ञा = पित् + ऋ + आज्ञा = पित् + र् + आज्ञा = पित्राज्ञा ।
नियम (घ) — यदि ‘लृ’ के बाद कोई असमान स्वर आये, तो ‘लृ’ का ‘ल्’ हो जाता है।
जैसे-
लृ + आ = ल् + आ = ला, लृ + आकृतिः = ल् + आकृतिः = लाकृतिः ।
नोट-ऊपर लिखे नियमों को एकत्र करने से निम्न नियम बनता है-यदि हस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ, लृ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ‘इ’ का ‘य्’, ‘उ’ का ‘व्’ ‘ऋ’ का ‘र्’ और ‘लृ’ का ‘ल्’ हो जाता है।
५. अयादि स्वर सन्धि
सूत्र- एचोऽयवायावः ।
नियम (क)– यदि ‘ए’ के बाद कोई स्वर आए, तो ए का ‘अय्’ हो जाता है।
जैसे-
ए + अ = अय् + अ = अय, ने + अनम् = न् + ए +अनम्+ न् + अय् + अनम् = नयनम् ।
ए + अ = अय् + ए = अये, हरे + ए = हर् + ए + अ = हर् + अय् + ए = हरये ।
नियम (ख) –यदि ‘ऐ’ के बाद कोई स्वर आये, तो ‘ऐ’ का आय् हो जाता है ।
जैसे-
ऐ + अ = आय् + अ + आय, नै+ अकः = न् + ऐ + अकः = न + आय् + अकः = नायकः ।
नियम (ग)– यदि ‘ओ’ के बाद कोई स्वर आए, तो ‘ओ’ का अव् हो जाता है ।
जैसे-
ओ + इ = अव् + इ = अवि, पो+ इत्रः = प्+ ओ + इत्रः = प् + अव् + इत्रः = पवित्रः ।
ओ + अ = अव् + ए = अवे, विष्णो + ए = विष्ण् + ओ + ए = विष्ण्+ अव् + ए = विष्णवे ।
नियम (घ)– यदि ‘औ’ के बाद कोई स्वर आए तो ‘औ’ का आव् हो जाता है।
जैसे-
औ + अ = आव् + अ = आव, पौ+ अकः = प्+ औ + अकः = प् + आव् + अकः = पावकः ।
अपवाद- जहाँ पदान्त के ‘ए’ या ‘ओ’ के बाद ‘अ’ आता है वहाँ अय् न होकर ‘अ’ को पूर्व रूप (ऽ) हो जाता है। जैसे- हरे + अव् = हरेऽव । विष्णो + अव = विष्णोऽव। इसे पूर्व रूप स्वर सन्धि कहते हैं।
नोट-उक्त नियमों को एकत्र करने से निम्न नियम बनता है-
यदि ए, ऐ और ओ, औ के बाद कोई स्वर आये तो ‘ए’ का ‘अय्’ ‘ऐ’ का ‘आय्’, ‘ओ’ का ‘अव्’ और ‘औ’ का ‘आव्’ हो जाता है।
६. पूर्वरूप स्वर सन्धि
सूत्र – एडः पदान्तादतिः ।
नियम- पदान्त में ‘ए’ अथवा ‘ओ’ के बाद ‘अ’ के आने पर ‘अ’ को पूर्वरूप (S) हो जाता है। जैसे-
हरे + अव = हरेऽव ।
विष्णो + अव = विष्णोऽव ।