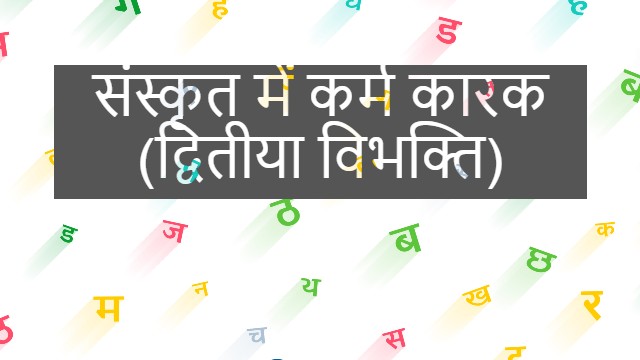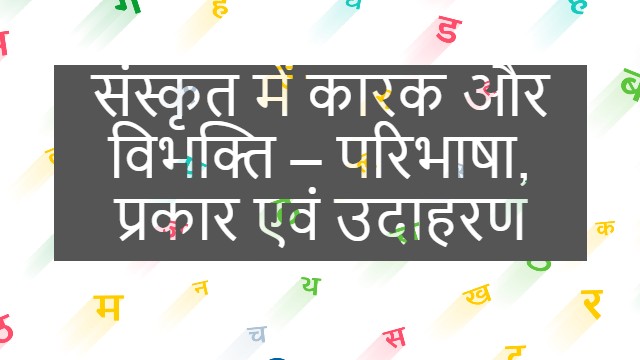२. कर्मकारक (द्वितीया विभक्ति)
१. सूत्र- “कर्तुरीप्सिततम कर्म कर्मणि द्वितीया”
अर्थात् जिसके ऊपर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, उसे कर्मकारक कहते हैं। जैसे- मैं राम को देखता हूँ। इस वाक्य में देखने के व्यापार का फल ‘राम’ पर पड़ रहा है, अतः ‘राम’ में कर्मकारक का चिन्ह ‘को’ है, किन्तु यह कभी-कभी छिपा भी रहता है। जैसे- राम पुस्तक पढ़ता है।
- कर्तृवाच्य में कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे- रामः ग्रन्थं पठति ।
- किन्तु कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति ही होती है। जैसे- रामेण ग्रन्थः पठ्यते । (राम के द्वारा ग्रन्थ पढ़ा जाता है।)
- गमनार्थक धातुओं के योग, जहाँ जाया जाता है, उसमें द्वितीया होती है, जैसे- रामः गृहं गच्छति (राम घर जाता है) छात्रः कक्षा प्रविशति (छात्र कक्षा में प्रवेश करता है।) सः वृक्षम् आरोहति (वह वृक्ष पर चढ़ता हैं।)
२. सूत्र- “अकथितं च”।
संस्कृत में सोलह धातुएँ तथा उनके अर्थ वाली दूसरी धातुएँ द्विकर्मक हैं, अतः इनके दो कर्म हैं। ये धातुएँ निम्न हैं-
- याच् (माँगना) – बालकः जनक मोदकं याचते (याचति)। (बालक पिताजी से लड्डू माँगता है ।)
- पच् (पकाना) – अहम् तण्डुलान् ओटनं पचामि । (मैं चावलों से भात पकाता हूँ।)
- प्रच्छ् (पूछना) – गुरुः छात्रं प्रश्नं पृच्छति । (गुरुजी विद्यार्थी से प्रश्न पूछते हैं।)
- ब्रू (बोलना, कहना) – आचार्यः शिष्यं धर्मं ब्रूते । (आचार्य शिष्य को धर्म का उपदेश देता है ।)
- नी (ले जाना) – सः ग्रामम् अजां नयति । (वह गाँव में बकरी ले जाता है।)
- दुह् (दुहना) – कृष्णः धेनुं दुग्धं दोग्धिः । (कृष्ण गाय से दूध दुहता है।)
- दण्ड (दण्ड देना, जुर्माना करना) – न्यायाधीशः चौरं सहस्रं दण्डयति । (न्यायाधीश चोर को हजार रुपयों का दण्ड देता है ।)
- रुघ् (घेरना, रोकना) – सः धेनुं मार्गम् अवरुद्धणि (वह गाय को रास्ते में घेरता है ।)
- चि (चयन करना, इकट्ठा करना, बटोरना) – सः पादपं पुष्पाणि, अवचिनोति । (वह पेड़ से फूलों को इकट्ठा करता है ।)
- शास् (शासन करना, कहना)- गुरुः शिष्यं धर्मम् शास्ति । (गुरुजी शिष्य को धर्म का शासन कहते हैं।)
- जि (जीतना) – देवदत्तः कृष्णं शतं रुप्यकाणि जयति । (देवदत्त कृष्ण से सौ रुपये जीतता है ।)
- मथ् (मथना) – सीता दुग्धं घृतं मथ्नाति । (सीता दूध से घी मथती है।)
- मुष् (चुराना) – चौरः कृष्णं शतं रुप्यकाणि मुष्णाति । (चोर कृष्ण के सौ रुपये चुराता है।)
- ह्र (हरण करना, चुराना) – चोरः रामं धनं हरति । (चोर राम का धन चुराता है।)
- कृष् (खोदकर निकालना) – जनः भूमिं रत्नानि कर्षन्ति । (मनुष्य भूमि से रत्न निकालते हैं।)
- वह् (ढोकर ले जाना) – भृत्यः ग्रामं भारं वहति । (नौकर गाँव को बोझ ले जाता है।)
३. सूत्र- “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे।”
समय तथा दूरी की निरन्तरता बतलाने वाले शब्दों में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे- क्रोशं कुटिला नदी। (नदी एक कोस तक टेढ़ी है।) रामः चतुर्दशवर्षाणि वने न्यवसत् । (राम १४ वर्ष तक वन में रहे।)
४. सूत्र- “अन्तरान्तरेण युक्ते”
निम्न शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है जैसे-
- बिना = सः पुस्तकं बिना कथं पठिष्यति (वह पुस्तक के बिना कैसे पढ़ेगा ?)
- अन्तरेण, ऋते = गोपालं बिना (अन्तरेण ऋते) कः तत्र गमिष्यति ? (गोपाल के बिना कौन वहाँ जायेगा ?)
- अन्तरा (बीच में) = रामं लक्ष्मणं च अन्तरा सीता अस्ति। (राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है)
५. सूत्र- “अधिशीङ् स्थासां कर्मः।”
नियम- यदि शीङ् (सोना), स्था (ठहरना) तथा आस् (बैठना) धातुओं से पहले ‘अधि’ उपसर्ग आये तो इसके आधार में द्वितीया होती है। जैसे-अधि + शीङ् = बालः शय्याम् अधिशेते । (बालक शय्या पर सोता है।) शय्या सोने का आधार है, अतः साधारण नियम के अनुसार इसमें सप्तमी होनी चाहिए किन्तु अर्धिशेते में अधिपूर्वक ‘शीङ्’ धातु है, अतः ‘शय्या’ में द्वितीया हुई है।
- अधि + स्था = रामः गृहम् अधितिष्ठति । (राम घर में स्थित है।) ‘अधितिष्ठति’ के साथ आने के कारण गृहम् में सप्तमी के स्थान पर द्वितीया
- अधि + आस् = राजा सिंहासनम् अध्यास्ते । (राजा सिंहासन पर बैठता है।) बैठने का आधार सिंहासन है, सामान्यतया यहाँ सप्तमी होनी चाहिए परन्तु अध्यास्ते के साथ आने से ‘सिंहासनम्’ में द्वितीया हुई है।
विशेष- यदि शीङ्, स्था, आस् धातुओं से पहले ‘अधि’ उपसर्ग नहीं होता है तो उनके आधार में सप्तमी होगी, द्वितीया नहीं। जैसे- बालः शय्यायां शेते, रामः गृहे तिष्ठति, राजा सिंहासने आस्ते ।
६. सूत्र- “अभितः परितः, समया, निकषा हाप्रतियोगेऽपि”
वार्तिक – उभ्सयर्वतसोः कार्याधिगुपर्या दिषु त्रिषु ।
द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ।।
- नियम – अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, समया, निकषाः, हा, प्रति आदि के योग में द्वितीया होती है।
- अभितः परितः सर्वतः – (चारों ओर) ग्रामम् अभितः (परितः, सर्वतः) वनम् अस्ति । (गाँव के चारों ओर वन हैं।)
- उभयतः – (दोनों ओर) विद्यालयम् उभयतः उद्यानम् अस्ति । (विद्यालय के दोनों ओर बगीचा है।)
- समया निकषा – (समीप) विद्यालयं समया (निकषा) गंगा अस्ति । (विद्यालय के समीप गंगा है।)
- प्रति – रामः सीतां प्रति उदारः आसीत् । (राम सीता के प्रति उदार थे ।)
- नियम – बिना (बिना) के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी होती है।
- बिना – रामं, रामेण, रामात् बिना दशरथः न अजीवत् । (राम के बिना दशरथ जीवित न रहे ।)